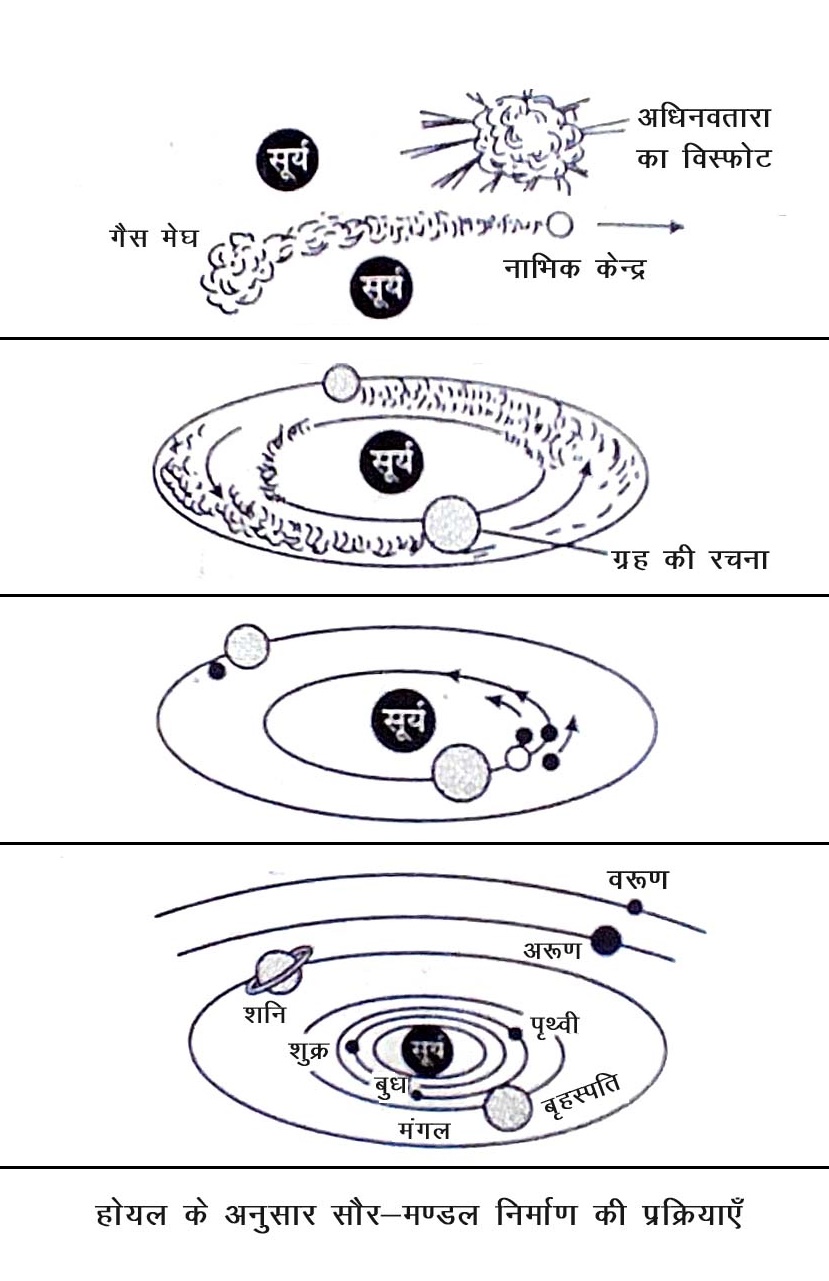लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धान्त Lothiyan green ka chatusfalak siddhant

लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धान्त लोथियन ग्रीन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सन् 1875 में किया। यह सिद्धान्त चतुष्फलक की सामान्य विशेषताओं पर आधारित है। चार बराबर भुजाओं वाले त्रिभुजों की आकृति चतुष्फलक कहलाती है। इसके त्रिभुज सपाट तथा चपटे धरातल वाले होते हैं। उनका सिद्धान्त अग्र तथ्यों पर आधारित है— एक गोलाकार आकृति अपने धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक आयतन रखती है। एक चतुष्फलक आकृति अपने धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा कम आयतन रखती है। लोथियन ग्रीन का सिद्धान्त फेयर बर्न की इस मान्यता पर आधारित है कि किसी गोलाकार पाइप को चारों ओर से समान दाब द्वारा दबाने पर वह चतुष्फलक की आकृति का हो जाता है। लोथियन ग्रीन का विचार है कि पृथ्वी प्रारम्भिक अवस्था में तरल थी जो धीरे-धीरे ठण्डा होने से ठोस रूप में परिवर्तित हुई। ठण्डे होने की इस प्रक्रिया में पृथ्वी का बाह्य भाग आन्तरिक भाग की तुलना में अधिक सिकुड़ गया। इस संकुचन से पृथ्वी के भीतरी भाग का आयतन भी कम हो गया तथा भूपृष्ठ एवं आन्तरिक भाग के मध्य कुछ स्थान रिक्त हो गया। इस आन्तरिक भाग पर इस ऊपरी भाग ने दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया। इस...